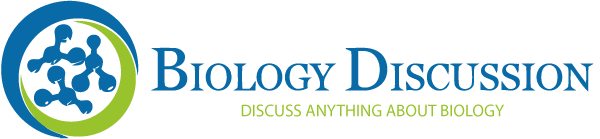ADVERTISEMENTS:
Read this article in Hindi to learn about the economic importance of arthropoda.
प्राणिजगत् के कुल प्राणियों में से लगभग 75% आर्थोपोडा समूह के है ।
आर्थोपोडा में कुल चार प्रकार के जन्तु-समूहों का समावेश है:
ADVERTISEMENTS:
1. वर्ग-क्रस्टेशिया (Crustacea):
केकड़े, झिंगे, आदि ।
2. वर्ग-मिरिआपोडा (Myriapoda):
सेन्टीपीड, मिलीपीड आदि।
ADVERTISEMENTS:
3. वर्ग-इन्सेक्टा (Insecta):
कॉकरोच, मच्छर, मक्खी, खटमल, जूं, मधुमक्खी, रेशम एवं लाख के कीड़े आदि ।
4. एरेकनिडा (Archnida):
मकड़ी, बिच्छू आदि ।
ये विभिन्न प्रकार के जन्तु मनुष्य समाज को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लाभ अथवा हानि पहुंचाते हैं ।
1. क्र्स्टेशिया जन्तुओं का आर्थिक महत्व:
इस समूह के अन्तर्गत आने वाले जन्तुओं में सैकड़ों प्रकार के केकड़े (crabs) एवं झिंगे (lobsters) प्रमुख हैं । माँसाहारी लोग इन्हें खाने के काम में लेते हैं । हमारे देश में भी समुद्र तटों पर लगभग 75 प्रकार के झिंगों का पालन-पोषण व्यापारिक स्तर पर किया जाता है ।
अनेक प्रकार के सूक्ष्म क्रस्टेशिया जन्तु-प्लवक (zooplankton झूप्लेंक्टॉन) के रूप में जलाशयों की ऊपरी सतह पर करोड़ों की संख्या में होते हैं । अनेक मछलियाँ एवं व्हेल प्राणी इन्हीं जन्तु-प्लवकों को खाते हैं । हम सब जानते हैं कि मछलियों का माँसाहारी लोगों के भोजन में कितना महत्व है ।
अत: मछली उत्पादन क्रस्टेशिया जन्तुओं पर निर्भर होता है । मछली पकड़ने के लिए भी क्रस्टेशिया जन्तुओं का चारे (bait) के रूप में उपयोग होता है । क्रस्टेशिया जन्तुओं से हमें कुछ हानि भी पहुँचती है । जैसे कुछ प्रकार के झिंगे जलीय पौधों एवं फसलों को नष्ट करते हैं ।
ADVERTISEMENTS:
कुछ समुद्री क्रस्टेशिया जंतु (लेपस, बेलेनस) आदि जहाजों पर लाखों की संख्या पर चिपके रहते हैं एवं दुर्गन्ध फैलाते हैं । इनकी साफ-सफाई पर भारी खर्च आता है । इसी प्रकार साइक्लोप्स एवं डेफ्निया जैसे सूक्ष्म-जन्तु अनेक प्रकार के रोगाणुओं के वाहक (disease carrier) का काम करते हैं । चिर परिचित नारू-रोग सायक्लोप्स जन्तु के माध्यम से ही एक मनुष्य से दूसरे में पहुँचता है ।
2. मिरिआपोडा जन्तुओं का आर्थिक महत्व:
इसके अन्तर्गत आने वाले जन्तु मुख्य रूप से सेन्टीपीड (कनखजूरे) एवं मिलिपीड हैं । ये जन्तु विशेष आर्थिक महत्व के नहीं होते । कुछ मिलिपीड पौधों की जड़ों को नुकसान पहुँचाते हैं । कनखजूरे के काटने से भी अत्यधिक दर्द होता है ।
3. एरेकनिडा जन्तुओं का आर्थिक महत्व:
ADVERTISEMENTS:
इस वर्ग में मुख्य रूप से सैकड़ों प्रकार के बिच्छुओं एवं मकड़ियों (बग्गी, चिचड़ी आदि) का समावेश है । बिच्छू जहाँ एक ओर अनेक प्रकार के हानिकारक कीड़ों को खाकर नष्ट करते हैं वहीं डंक से विष शरीर के भीतर पहुँचाकर हमें दर्द भी पहुँचाते हैं । बिच्छू के विष का औषधि हेतु भी उपयोग होता है ।
अनेक प्रकार की बग्गी (mites) एवं चिचड़ी (ticks) हमारे पालतू पशुओं एवं पक्षियों पर बाह्य-परजीवी के रूप में रहती हैं । उन पशु-पक्षियों को काटकर, उनका खून चूसकर नुकसान करती हैं । इन पशुओं की त्वचा पर इनके कारण से घाव हो जाते हैं । इन घावों से अनेक प्रकार के रोगाणु भी प्रवेश कर जाते हैं ।
4. इन्सैक्टा-वर्ग के जन्तुओं (कीटों) का आर्थिक महत्व:
कुल आर्थोपोडा जन्तुओं में लगभग 90 प्रतिशत जन्तु कीटवर्ग के होते हैं । कीटवर्ग के जन्तुओं का मनुष्य की अर्थव्यवस्था से घनिष्ठ संबंध है । अनेक प्रकार के कीट फसलों, पुस्तकों, जंगलों एवं अनाज को नष्ट करते हैं । कुछ कीट अनेक प्रकार की बीमारी फैलाने में मदद करते हैं । वहीं दूसरी ओर रेशम, शहद, लाख जैसी बहुमूल्य वस्तुएँ हमें कीटों से ही प्राप्त होती हैं ।
हानिकारक कीट:
ADVERTISEMENTS:
(a) विषैले कीट:
अनेक प्रकार के कीट एवं उनके लार्वा में विषैले पदार्थ होते हैं । मधुमक्खी, भौरी (बर्र-Vasp), चींटी, ऐसे ही कीट हैं । कुछ मक्खियाँ एवं मच्छर त्वचा भेदकर कष्ट पहुँचाते हैं ।
(b) फसलनाशक कीट:
कीटवर्ग के जन्तु फसलों को अनेक प्रकार से हानि पहुँचाते हैं:
ADVERTISEMENTS:
(1) पौधों की पत्तियाँ, फलियाँ, कलियां एवं तने को खाकर अथवा रस चूसकर:
पौधों के विभिन्न भागों को खाकर नष्ट करने वाले कीटों में टिड्डे (grass-hoppers), टिड्डियाँ (locusts), गुबरैले (beetles), पत्तागोभी के कीड़े (cabbageworm), एवं झिंगुर प्रमुख हैं । टिड्डी दल तो करोड़ों की संख्या में एक साथ-उड़ते हैं । रात में ये विश्राम करते हैं । जिस खेत में ये रात को विश्राम करते हैं वहाँ की फसल को पूरी चौपट कर देते हैं ।
रस चूसने वाले कीटों में अनेक प्रकार के एफिड (aphids) एवं कपास के लाल कीड़े जैसे कीट प्रमुख हैं ।
(2) पौधों के विभिन्न भागों में छेद करने वाले कीट:
ADVERTISEMENTS:
ये कीट पौधों के तनों, जड़ों, फलों आदि में अंडे देते हैं । अंडे से निकले लार्वा उन भागों के रस को चूसकर पूरे पौधे को नष्ट कर देते हैं । इन कीटों को नष्ट करना भी मुश्किल होता है । गन्ने का माथ (Sugarcane moth), पाइरिला (Pyrilla), चावल की गंधी (Rice bug), कपास की शुंडी (Cotton weevil), आलू, खीरे आदि फसलों के गुबरैल (bettles) मुख्य रूप से छेद कर नुकसान पहुँचाने वाले कीट हैं ।
(3) पौधों में कैंसर करने बाले कीट:
ये गॉल कीड़े कहलाते हैं । ये पौधों में बड़ी-बड़ी गठानें उत्पन्न कर पौधों की सामान्य वृद्धि रोक देते हैं । इनमें मुख्य रूप से गेहूँ का गॉल (wheat joint worm) एवं अंगुर का गॉल (grape phylloxera) अत्यन्त हानिकारक है ।
(4) जड़ नष्ट करने बाले:
इनमें सेवफल के पेड़ की जड़ों से रस चूसने वाला ‘वूली एफिड’ (wooly apple aphid) एक मुख्य कीट है जो शिशु एवं वयस्क दोनों ही अवस्थाओं में जड़ों से रस चूसकर पेड़ को जमीन के खनिज तत्व नहीं मिलने देता । इस तरह से पेड़ बेकार हो जाते हैं ।
ADVERTISEMENTS:
(c) मवेशियों के लिए हानि कारक कीट:
मवेशियों को हानि पहुंचाने वाले कुछ कीटों की जानकारी निम्न है:
(d) मुर्गी पालन में हानिकारक कीट:
मुर्गी- पालन में सबसे अधिक तकलीफ पहुँचाने वाले विभिन्न कीट हैं, जो कई तरह की बीमारियाँ फैलाते हैं । इनमें से ‘रानी खेत’ नाम की बीमारी प्रमुख हैं । इसके अतिरिक्त इन्हें चेचक, काक्सीडियोसिस, किलनी बुखार, हैजा, सफेद दस्त व खून की कमी आदि प्रमुख रोग हैं ।
उपरोक्त वर्णित रोगों के कारण इन पर पाये जाने वाली कीट हैं, जिनमें से मुख्य कीट पॉल्ट्री लाइस (poultry lice), ‘फाऊल टिक’ (fowl tick), चिकन माइट (chicken mite) इत्यादि हैं ।
(e) संग्रहित अनाज को नष्ट करने बाले कीट:
(1) सुंडी अथवा घुन:
यह गहरे लाल रंग का कीट होता है, जिसका सिर एक तुण्ड (snout) के रूप में आगे की ओर निकला रहता है । इसका वैज्ञानिक नाम साइटोफिलस ग्रेनेरियस (Sitophilus granarious) एवं चावल की सूंडी का वैज्ञानिक नाम साइटोफिलस ओराइजा (Sitophilus oryza) है । इस कीट के लार्वा (डिम्भ) एवं वयस्क दोनों ही गेहूँ अथवा चावल को खाकर उसे खोखला कर देते हैं ।
(2) आटे के कीड़े (Meal worm-tenebrio molitor):
ये कीट आटे में रहकर उसे खाते हैं।
(3) फ्लोर माथ (Flour moth):
इनकी मादा मॉथ आटे में अंडे देती है । इन अंडों से निकले डिम्भ आटा खाने के साथ-साथ एक चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं । जिससे आसपास का आटा चिपक कर एक नली जैसा बन जाता है । इस तरह से आटा-मिलों के ये खास दुश्मन हैं ।
(4) खपरा बीटल (Khapra bettle- Trogoderma granarium):
वह भी गहरे लाल रंग का गोल कीट होता है । इसके डिम्भ हल्के भूरे रंग के होते हैं । ये गेहूं, ज्वार, मक्का आदि को नुकसान पहुँचाते हैं ।
(5) दालों का घुन (Pulse bettle):
यह गहरे लाल अथवा चाकलेट रंग के होते हैं । यह सभी प्रकार की दालें, जैसे- मटर, मूँग, अरहर, उड़द, चना, मसूर में पाये जाते हैं । इस कीट की मादाएँ खड़ी फसल पर ही फलियों पर अंडे देती हैं । इन अंडों से निकले लार्वा फलियों के भीतर घुसकर बीजों को खाते हैं एवं उनमें छेद कर देते हैं । छिद्र करके ये डिम्भ दानों के भीतर ही बन्द हो जाते हैं । दाने के भीतर ही ये लार्वा वयस्क होते हैं एवं पूर्ण दाने को खोखला कर देते हैं ।
(f) कपड़े एवं पुस्तक नाशक कीट:
कपड़ों एवं पुस्तकों को नष्ट करने वाले कीटों में कॉकरोच, दीमक, क्लॉथ मॉथ, कारपेट बीटल (Carpet beetle) एवं बुक लाइस (Book lice) मुख्य हैं ।
क्लॉथ मॉथ के लार्वा ऊनी वस्त्र, पंखों एवं फर से बने वस्त्रों को खाकर उनमें असंख्य छोटे-छोटे छिद्र कर देते हैं । कई दिनों तक बक्सों में बन्द रखे कपड़े जिनका उपयोग नहीं होता, उन्हें कारपेट बीटल के डिम्भ (लार्वा) खाकर नष्ट करते हैं । पुस्तकों की सबसे बड़ी दुश्मन दीमक है, क्योंकि इनका मुख्य भोजन सैलुलोस है । दीमक के अलावा अत्यन्त छोटे-छोटे बिना पंख वाले की भी पुस्तकों को नष्ट करते हैं जिन्हें ‘बुक लाइस’ कहते हैं ।
(g) मनुष्य में रोग फैलाने बाले कीट:
मनुष्य को सबसे अधिक हानिक पहुँचाने वाले अनेक कीट हैं जो अनजाने ही कई भयंकर रोगों के रोगाणु एक रोगी से दूसरे रोगी तक पहुँचाने का कार्य करते हैं ।
यह कार्य मुख्यरूप से निम्नलिखित कीटों द्वारा किया जाता है:
(1) मच्छर (mosquitoes):
मच्छर मनुष्य का रक्त चूसते समय अनेक बीमारियों के रोगाणुओं को, जो उनमें होते हैं मनुष्य के रक्त प्रवाह में छोड़ देते हैं । इनके द्वारा फैलाई गई बीमारियों में मलेरिया, फाइलेरिया, हाथी पाँव आदि मुख्य हैं ।
(2) मक्खियाँ (House files):
ये किसी रोगी द्वारा उत्सर्जित मल पर बैठकर वहाँ से रोगाणु अपने शरीर पर रखकर उसे मनुष्य के अन्य खाद्यान्नों पर छोड़ देती हैं जिसे ग्रहण कर अन्य स्वस्थ मनुष्य भी रोगी हो जाता है । मक्खी को ‘रोगों की चलती फिरती गाड़ी’ भी कहते हैं ।
इसके द्वारा फैलाये जाने वाले रोगों में हैजा, पेचिस, मियादी बुखार, ट्रोकोमा (trochoma) इत्यादि मुख्य हैं । घरेलू मक्खी के अलावा अन्य मक्खियाँ भी कई रोग फैलाती हैं, जैसे- सेटसी मक्खी (tse-tse fly) अफ्रीका में स्लीपिंग सिकनेस (sleeping sickness) नामक रोग करती है, जिसका कोई इलाज नहीं है ।
(3) जूँ (Body louse):
ये मनुष्य के बाह्य परजीवी के रूप में रहकर मनुष्य का खून चूसती हैं एवं टाइफस (typhus), ट्रेंच ज्वर (Trench fever) तथा रेलेप्सिंग ज्वर (relapsing fever) नामक रोग फैलाती हैं ।
(4) खटमल (Bed bug):
ये भी मनुष्य का रक्त चूसते हैं एवं दक्षिण अमेरिका में ये ‘चागा’ (chage) बीमारी फैलाते हैं । हमारे देश में ये कालाजार (Kalazar) नामक ज्वर फैलाते हैं ।
(5) पिस्सु (Fleas):
पिस्सु विभिन्न प्राणियों के शरीर पर बाह्य-परजीवी के रूप में रहते हैं । चूहे के शरीर पर रहने वाला पिस्सु जेनोप्सिला किओपिस (Xenopsyllacheopis) प्लेग के रोगाणु फैलाता है ।
लाभदायक कीट:
यद्यपि हजारों प्रकार के हानिकारक कीटों से हमें बहुत हानि होती है किन्तु लाभ भी कोई कम नहीं है ।
प्रमुख लाभ निम्न प्रकार से हैं:
(a) उत्पादक कीट:
मधुमक्खी, रेशम के कीड़े एवं लाख के कीड़े से हमें क्रमश: मधु (शहद), रेशम एवं लाख मिलता है । मधु एपिस वंश (genus-Apis) की कुछ जातियाँ अपने छत्ते में बनाती हैं । छत्ते से मधु के अलावा उपयोगी मोम (Bees wax) भी मिलता है । मधु एक अमूल्य खाद्य-पदार्थ तो है ही, महत्वपूर्ण औषधि भी है ।
रेशम का उत्पादन बाम्बिक्स वंश (Genus-bombyx) के पतंगों (moths) द्वारा किया जाता है । प्रति वर्ष संसार में 2.5 लाख क्विंटल रेशम के कपड़े का उपयोग होता है । लाख एक ट्रेकार्डिया लेका (Trachardia lacca) एवं लेसिफर लेका नामक कीट की मादा कीटों द्वारा स्रावित पदार्थ होता है ।
लाख से अनेक व्यापारिक वस्तुओं का उत्पादन (जैसे ग्रामोफोन की रेकार्ड, स्याही, चुड़ियाँ, वार्निश आदि) होता है । हमारे प्रदेश में लाख एवं रेशम का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता है । संसार का कुल कच्चे लाख का उत्पादन लगभग 40 करोड़ किलो है ।
(b) कीटों द्वारा पौधों में परागण (Pollination):
पौधों में परागण क्रिया सम्पन्न करवाने में कीटों की प्रमुख भूमिका होती है । फूलों का मकरन्द लेते समय नर पुष्पों के परागकण भी कीटों के शरीर पर चिपक जाते हैं । जब ये कीट अन्य फूल पर जाते हैं तब मादा जननांगों पर उक्त परागकण छिड़क देते हैं एवं इस तरह परागण करवाने में सहायक होते हैं ।
मधुमक्खियाँ, भौरियाँ, भौरे, मक्खियाँ, चीटियाँ, तितलियाँ, पतंगे जैसे कीट परागण की भूमिका करवाने वाले मुख्य कीट हैं । शोधकार्यों से विदित हुआ है कि खेतों में मधुमक्खी पालने से फसल उत्पादन अधिक होता
है ।
(c) अपमार्जक कीट (Scavangers):
अनेक कीट जैसे सिल्वर फिश, दीमक, चीटियाँ, घरेलू मक्खियां, अनेक गुबरैले, लार्वा, कॉकरोच आदि मृत जन्तुओं एवं गिरी पत्तियाँ फल आदि खाकर वातावरण की सफाई करते है । इससे मृत वस्तु को सड़ने का मौका नहीं मिलता ।
(d) जैव-नियन्त्रण (Biological control):
कुछ कीट अन्य हानिकारक कीटों को नष्ट करने का काम करते हैं । कीटों के ऐसे नियन्त्रण को जैव-नियन्त्रण कहते हैं । कुछ हानिकारक कीटों को खाकर नष्ट करते हैं एवं कुछ हानिकारक कीटों में परजीवियों में रहकर नष्ट करते हैं ।
(e) भोजन के रूप में कीटों का उपयोग:
असंख्य पक्षी, मेंढक मछली छिपकली आदि कीड़ों को अपना भोजन बनाते हैं । कुछ पिछड़े देशों की जंगली जातियों के लोग अनेक प्रकार के कीटों एवं उनके अंडों को खाते हैं ।
(f) औषधि में कीटों का उपयोग:
प्राचीन समय में मक्खियों के मैगट लार्वा (Maggots) संक्रमण के इलाज हेतु उपयोग में लिये जाते थे । मधुमक्खी का विष गठिया के इलाज के लिए उपयोग में लिया जाता था । शहद भी एक तरह का एन्टी सेप्टिक (antispetic) का काम करता है । कैन्थ्रेडीन भी ब्लिस्टर कीट से बनता है ।